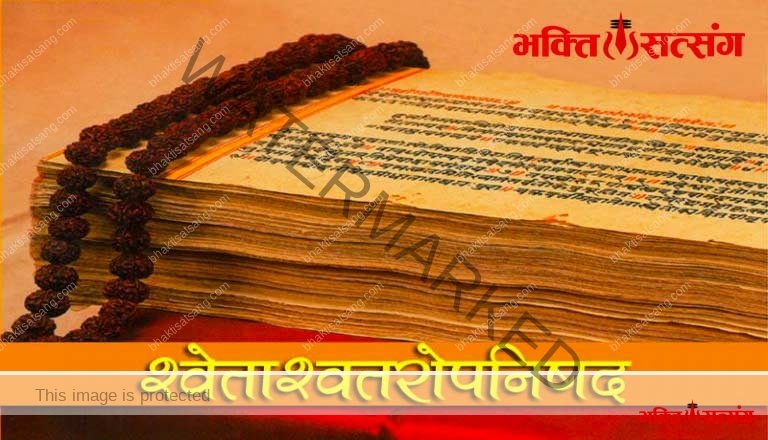कृष्ण यजुर्वेद शाखा के इस उपनिषद में छह अध्याय हैं। इनमें जगत का मूल कारण, ॐकार-साधना, परमात्मतत्त्व से साक्षात्कार, ध्यानयोग, योग-साधना, जगत की उत्पत्ति, संचालन और विलय का कारण, विद्या-अविद्या, जीव की नाना योनियों से मुक्ति के उपाय, ज्ञानयोग और परमात्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है।
प्रथम अध्याय
इस अध्याय में जगत के मूल कारण को जानने के प्रति जिज्ञासा अभिव्यक्त की गयी है। साथ ही ‘ॐकार’ की साधना द्वारा ‘परमात्मतत्त्व’ से साक्षात्कार किया गया है। काल, स्वभाव, सुनिश्चित कर्मफल, आकस्मिक घटना, पंचमहाभूत और जीवात्मा, ये इस जगत के कारणभूत तत्त्व हैं या नहीं, इन पर विचार किया गया है। ये सभी इस जगत के कारण इसलिए नहीं हो सकते; क्योंकि ये सभी आत्मा के अधीन हैं।
आत्मा को भी कारण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह सभी सुख-दु:ख के कारणभूत कर्मफल-व्यवस्था के अधीन है। केवल बौद्धिक विवेचन से ‘ब्रह्म’ को बोध सम्भव नहीं है। ध्यान के अन्तर्गत आत्मचेतन द्वारा ही गुणों के आवरण को भेदकर उस परमतत्त्व का अनुभव किया जा सकता है।
सम्पूर्ण विश्व-व्यवस्था एक प्रकृति-चक्र के मध्य घूमती दिखाई देती है, जिसमें सत्व, रज, तम गुणों के तीन वृत्त हैं, पाप-पुण्य दो कर्म हैं, जो मोह-रूपी नाभि को केन्द्र मानकर घूमते रहते हैं। इस ब्रह्मचन्द्र’ में जीव भ्रमण करता रहता है। इस चक्र से छूटने पर ही वह ‘मोक्ष’ को प्राप्त कर पाता है। उस परमात्मा को जान लेने पर ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है।
वह ‘परमतत्त्व’ प्रत्येक जीव में स्थित है। मनुष्य अपने विवेक से ही उसे जान पाता है। वह जीव और जड़ प्रकृति के परे परमात्मा है, ब्रह्म है।’ओंकार’ की साधना से जीवात्मा, परमात्मा से संयोग कर पाता है। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, काष्ठ में अग्नि, स्रोत में जल छिपा रहता है, उसी प्रकार परमात्मा अन्त:करण में छिपा रहता है। ‘आत्मा’ में ही ‘परमतत्त्व’ विद्यमान रहता है।
दूसरा अध्याय
इस अध्याय में ‘ध्यानयोग’ द्वारा साधना पर बल दिया गया है। योग-साधना और ‘प्राणायाम’ विधि द्वारा ‘जीवात्मा’ और ‘परमात्मा’ को संयोग होता है। इस संयोगावस्था को प्राप्त करने के लिए साधक सूर्य की उपासना करते हुए ‘ध्यानयोग’ का सहारा लेता है। वह स्वच्छ स्थान पर बैठकर प्राणायाम विधि से अपनी आत्मा को जाग्रत करता है और उसे ‘ब्रह्मरन्ध्र’ में स्थित ब्रह्म-शक्ति तक उठाता है।
इन्द्रियों की समस्त सुखाकांक्षाएं अन्त:करण में ही जन्म लेती हैं। उन्हें नियन्त्रित करके ही ‘ओंकार’ की साधना करनी चाहिए। जिस प्रकार सारथि चपल अश्वों को अच्छी प्रकार साधकर उन्हें लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष इस ‘मन’ को वश में करके ‘आत्मतत्त्व’ का सन्धान करे।
जो साधक, पंचमहाभूतों से युक्त गुणों का विकास करके ‘योगाग्निमय’ शरीर को धारण कर लेता है, उसे न तो रोग सताता है, न उसे वृद्धावस्था प्राप्त होती है। उसे अकालमृत्यु भी प्राप्त नहीं होती। योग-साधना से युक्त साधक आत्मतत्त्व के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करता है। तब वह सम्पूर्ण तत्त्वों में पवित्र उस परमात्मा को जानकर सभी प्रकार के विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।
तीसरा व चौथा अध्यायतीसरे और चौथे अध्याय में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संचालन और विलय में समर्थ परमात्मा की शक्ति की सर्वव्यापकता को वर्णित किया गया है। उसे नौ द्वार वाली पुरी में, इन्द्रियविहीन होते हुए भी सब प्रकार से समर्थ, लघु से लघु और महान से भी महान कहा गया है। ‘जीवात्मा’ और ‘परमात्मा’ की स्थिति को एक ही डाल पर बैठे दो पक्षियों के समान बताया गया है, जो मायावी ब्रह्म के मुक्ति-फल को अपने-अपने ढंग से खाते हैं।
सम्पूर्ण शक्तियों और लोकों पर शासन करने वाले उस मायावी ब्रह्म को, जो जान लेता है और उसे सृष्टि का नियामक समझता है, वह अमर हो जाता है। वह एक परमात्मा ही ‘रुद्र’ है, ‘शिव’ है। वह अपनी शक्तियों द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर शासन करता है।
सभी प्राणी उसी का आश्रय लेते हैं। और वह सभी प्राणियों में प्राण-सत्ता के रूप में विद्यमान है। वह पंचमहाभूतों द्वारा इस सृष्टि का निर्माणकर्ता है। उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। सम्पूर्ण विश्व उसी परमपुरुष में स्थित है और वह स्वयं समस्त प्राणियों में स्थित है। वह परमपुरुष समस्त इन्द्रियों से रहित होने पर भी, उनके विशेष गुणों से परिचित है। वह प्रकाश-रूप में नवद्वार वाले देह-रूपी नगर में अन्तर्यामी होकर स्थित है। वही बाह्य जगत की स्थूल लीलाएं कर रहा है। वह आत्म-रूप जीव, देह के हृदयस्थल पर विराजमान है।
ऋषि उस परमपिता को अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा और शुक्र नक्षत्र के रूप में जानता है। सृष्टि के प्रारम्भ में वह अकेला ही था, रंग-रूप से हीन था। वह अकारण ही अपनी शक्तियों द्वारा अनेक रूप धारण कर सकता है। सम्पूर्ण विश्व का जनक भी वही है और उसका विलय भी वह अपनी इच्छा से कर लेता है। वह स्वयं ‘दृश्य’ होकर भी ‘दृष्टा’ है। वह ‘आत्मा’ है और परमात्मा भी है। दोनों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। उसे इस उदाहरण द्वारा समझिये-
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरत्नय: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्योऽभिचाकशीति॥-(चतुर्थ अध्याय 6)
अर्थात संयुक्त रूप और मैत्री-भाव से रहने वाले दो पक्षी-‘जीवात्मा’ और ‘परमात्मा’- एक ही वृक्ष का आश्रय लिये हुए हैं। उनमें से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फलों, अर्थात कर्मफलों को स्वाद ले लेकर खाता है, किन्तु दूसरा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है।
राग-द्वेष, मोह-माया से युक्त होकर जीवात्मा सदैव शोकग्रस्त रहता है, किन्तु दूसरा सभी सन्तापों से मुक्त रहता है। यह प्रकृति उस मायापति परमात्मा की ही ‘माया’ है। वह अकेला ही समस्त शरीरों का स्वामी है तथा जीव को उनके कर्मों के अनुसार चौरासी लाख योनियों में भटकाता रहता है।
प्रत्येक काल में वही समस्त लोकों का रक्षक है, सम्पूर्ण जगत का स्वामी है और सभी प्राणियों में स्थित है। उस परम पुरुष को जानकर साधक अपने कर्म-बन्धनों से छूट जाता है।
पांचवां व छठा अध्याय
इन दोनों अध्यायों में विद्या-अविद्या, परमात्मा की विलक्षणता, जीव की कर्मानुसार विविध गतियों औ उनकी मुक्ति के उपाय बताये गये हैं। यहाँ जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्मतत्त्व की स्थापना की गयी है तथा ध्यान, उपासना और ज्ञानयोग द्वारा परमात्मा की सर्वव्यापकता और सामर्थ्य को जानने पर बल दिया गया है। अन्त में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा सुपात्र और योग्य व्यक्ति को ही देनी चाहिए।
विद्या–अविद्या
नश्वर जगत का ज्ञान ‘अविद्या’ है और अविनाशी जीवात्मा का ज्ञान ‘विद्या’ है। जो विद्या और अविद्या पर शासन करता है, वही परमसत्ता है। वह समस्त योनियों का अधिष्ठाता है। विद्या-अविद्या से परे वह परमतत्त्व है। वह सम्पूर्ण जगत का कारण है। वह ‘परब्रह्म’ है। वह जिस शरीर को भी ग्रहण करता है, उसी के अनुरूप हो जाता है।
वह सर्वज्ञ है।
जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है, जो ज्ञान-स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, काल का भी काल और सर्वगुणसम्पन्न अविनाशी है, जिसके अनुशासन में यह सम्पूर्ण कर्मचक्र सतत घूमता रहता है, सभी पंचतत्त्व जिसके संकेत पर क्रियाशील रहते हैं, उसी परब्रह्म परमात्मा का सदैव ध्यान करना चाहिए।
जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को प्रारम्भ करके उन्हें परमात्मा को अर्पित कर देता है, उसके पूर्वकर्मों का नाश हो जाता है और वह जीवात्मा जड़ जगत से भिन्न, उस परमसत्ता को प्राप्त हो जाता है। उस निराकार परमेश्वर के कोई शरीर और इन्द्रियां नहीं हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और विशाल से भी विशाल है। वह सब प्राणियों में अकेला है-
एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवली निर्गुणश्च॥ -(छठा अध्याय-11)
अर्थात सम्पूर्ण प्राणियों में वह एक देव (परमात्मा) स्थित है। वह सर्वव्यापक, सम्पूर्ण प्राणियों की अन्तरात्मा, सबके कर्मों का अधीश्वर, सब प्राणियों में बसा हुआ (अंत:करण में विद्यमान), सबका साक्षी, पूर्ण चैतन्य, विशुद्ध रूप और निर्गुण रूप है।
वस्तुत: इस लोक में एक ही हंस है, जो जल में अग्नि के समान अगोचर है। उसे जानकर साधक मृत्यु के बन्धन से छूट जाता है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान केवल योग्य साधक को ही देना चाहिए।